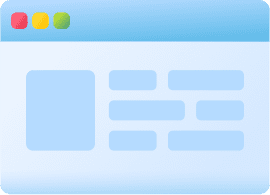महर्षि दयानन्द के वेदभाष्य की विशेषतायें◼️ ✍🏻 ल...

महर्षि दयानन्द के वेदभाष्य की विशेषतायें◼️ ✍🏻 लेखक - पदवाक्यप्रमाणज्ञ पण्डित ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु प्रस्तुति - 🌺 ‘अवत्सार’ परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से महापुरुष दयानन्द का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि जगन्नियन्ता अन्तर्यामी जगदीश्वर पर पूर्ण निष्ठावान होने के कारण ही उनको दैवी अन्तप्रेरणा हुई कि तुम वेद और वेदार्थ के सच्चे स्वरूप को संसार के सामने रक्खो, जिससे शताब्दियों से इस विषय की फैली हई भ्रान्ति दूर होकर विश्व का कल्याण हो। दयानन्द ने घोषणा की - वेद प्रभु की पवित्र वाणी है, जो सृष्टि के आदि में जीवों के कल्याणार्थ संसार के अन्य योग्य पदार्थों की भांति कर्मों की यथार्थ व्यवस्था के ज्ञानार्थ तदनुसार आचरण करने के लिए परम पवित्र ऋषियों द्वारा प्रदान की गई है। भावी कल्प-कल्पान्तरों में भी यह वाणी इसी प्रकार प्रादुर्भूत होगी। यह किसी व्यक्ति या व्यक्तिविशेषों की कृति नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व के रचयिता परमपिता परमात्मा की ही रचना है। इसमें किसी प्रकार की न्यूनाधिकता कल्प-कल्पान्तरों में नहीं होती। 🔥धाता यथापूर्वमकल्पयत्। ऋग्० १०।१९० समस्त संसार तथा तत्वसम्बन्धी ज्ञान, यह सब विधाता की यथापूर्व कृति है। यह है वेद के सम्बन्ध में वैदिकर्मियों की धारणा। यथार्थता की कसौटी पर ठीक उतरने से वैदिकर्मियों ने इस धारणा को अङ्गीकार किया है और उसके पुनरुद्धार का भार अपने ऊपर लिया है। वेद के इस स्वरूप को निर्धारित करने में वीतराग तपस्वी दयानन्द को कहां तक परिश्रम करना पड़ा, वह भी उस अवस्था में जबकि वेदों का पठन-पाठन लुप्त प्राय ही हो रहा था, इसके कहने की आवश्यकता नहीं। शास्त्र सम्बन्धी विविध रूढियों, प्रचलित रीतियों और शास्त्रकारों के कहे जानेवाले परस्पर विरोध की काली घटाओं, विविधवादों तथा मत-मतान्तरों के तूफान (झंझा) में दयानन्द चट्टान की तरह अविचल रहे। हम तो जब उस भयङ्कर तूफान का ध्यान करते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। उस तूफान में दयानन्द डिगे नहीं, अपने आपको दृढ़ता से सम्भाले रहे। इतना ही नहीं, अपितु उन्होंने एकदम इन सब परस्पर विरुद्ध रूढ़ियों और वादों के विरुद्ध घोषणा कर दी कि ‘वेद प्रभु की वाणी है, नित्य स्वतःप्रमाण है, इसमें किसी का इतिहास नहीं, अन्य सब शास्त्र वेदानकूलतया ही प्रमाण हैं।’ कल्पनामात्र से नहीं, अपितु प्रमाण और तर्क के आधार पर। ऋषि दयानन्द की इन धारणाओं का विशद निरूपण हमें उनकी 'ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका' में बहुत उत्तम रीति से मिलता है। वेदविषय का यह एक अपूर्व ग्रन्थ है, जिसमें वेदविषय की सभी आवश्यक बातों का समावेश है, जो कि वेद का स्वाध्याय करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को जाननी चाहिये। उसको पढ़ने के पश्चात् ही उनके वेदभाष्य की प्रक्रिया ठीक तरह समझ में आ सकती है। यद्यपि इस वेदभाष्य का वास्तविक स्वरूप स्वयं पढ़ने पर ही बुद्धिगत होगा तथापि हम ऋषि दयानन्दकृत भाष्य की कुछ विशेषताएं दर्शाते हैं, जिससे पाठकों को इस विषय का ज्ञान सुगमता से हो सके। ◼️दयानन्द-भाष्य की विशेषतायें- ◾️(१) यह वेद-भाष्य वेदापौरुषेयत्वाद की धारणा के आधार पर है। इस वेदभाष्य में कहीं पर भी इस धारणा के विरुद्ध कुछ नहीं मिलेगा। वेद पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर द्वारा प्रदत्त होने से पूर्ण ज्ञान है। इसमें अज्ञान का लेश भी नहीं। ◾️(२) इसमें लौकिक और वैदिक शब्दों के भेद को ध्यान में रखकर यास्क-पाणिनि-पतञ्जलि आदि ऋषि-मुनियों के आधार पर वेद के शब्दों के लिए समस्त वैदिक नियमों का आश्रयण किया गया है। ◾️(३) वेद में पाए नाम शब्दों को धातुज [यौगिक] मानकर [जैसा कि यास्क और पतञ्जलि का सिद्धान्त है] प्रकरणादि के आधार पर उन के सभी सम्भव अर्थों का निरूपण किया गया है। निर्वचन भेद से भिन्न भिन्न अर्थों का निरूपण भी इसमें मिलता है। ◾️(४) धातुओं के अनेकार्थत्व का सिद्धान्त जो सभी वैयाकरणों का मुख्य सिद्धान्त है, जिसको प्रायः सब वेदभाष्यकारों ने अपने भाष्यों में माना है, उसके आधार पर मन्त्रों के अर्थ किये गये हैं। ◾️(५) आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधियज्ञादि तीनों प्रक्रियाओं के आधार पर वेदमन्त्रों के अर्थ होते हैं, इस सिद्धान्त के अनुसार दयानन्दभाष्य के संस्कृत पदार्थ में प्राय: सभी प्रक्रियाओ में अर्थ दर्शाया गया ◾️(६) अनेक स्थानों में वैदिक पदों के अर्थ वेदमन्त्रों के आधार पर किये गये हैं। जैसे यजुर्वेद अध्याय १ मन्त्र १३ को देखिये। ◾️(७) अग्नि शब्द से केवल भौतिक अग्नि का ही ग्रहण नहीं होता, अपितु 'अग्नि' शब्द के निर्वचन के आधार पर आध्यात्मिक, आधिदैविक प्रक्रिया में परमेश्वर, विद्वान्, राजा, सभाध्यक्ष, नेता आदि तथा विद्युत्प्रकाश, जठराग्नि आदि का भी ग्रहण होता है। इसी प्रकार वायु, आदित्य, इन्द्र, यम, रुद्र आदि शब्दों के विषय में भी समझना चाहिये। और ये इन्द्र, वरुण, मरुत्, अग्नि, वायु, मित्र आदि शब्द जहां भौतिक पदार्थों के नाम हैं, वहां मुख्य वृत्ति से ईश्वर के वाची हैं। यह प्रक्रिया सारे भाष्य में बराबर मिलेगी। सबसे बड़ा मौलिक भेद दूसरे भाष्यों से इस भाष्य में यही है। यही इसका मूलाधारभूत वाद वा सिद्धान्त है, जिसको लक्ष्य में रखकर इस भाष्य की रचना हुई है। ◾️(८) इसमें 🔥'बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे' (वैशेषिकदर्शन ६।१।१) अर्थात् 'वेद में कोई बात तर्क के विरुद्ध नहीं है' इस सिद्धान्त के अनुसार वेद मन्त्रों का अर्थ किया गया है। ◾️(९) यास्क, पाणिनि, पतञ्जलि आदि के दर्शाये नियमानुसार अनेक स्थानों में प्राचीन कहे जानेवाले पदपाठों से भिन्न पद विभाग भी इस वेदभाष्य में दर्शाये गए हैं। 🔥'यथाभिमतदृष्टयो व्याख्यातणाम्' अर्थात् व्याख्या करने वालों की भिन्न-भिन्न दृष्टियां होती हैं। 🔥'न लक्षणेन पदकारा अनुवर्त्त्याः, पदकारैर्नम लक्षणमनुवर्त्यम्' (महाभाष्य ३।१।१०९) अर्थात् पदकारों के पीछे सूत्रकार नहीं चलेंगे, अपितु पदकारों को व्याकरण के पीछे चलना होगा। अतः इस भाष्य में व्याकरणानुसार पदकारों से भिन्न पद-विभाग भी माना गया है। वेद में अर्थ के पीछे स्वर है न कि स्वर के पीछे अर्थ। स्वर के अनुसार ही अर्थ हो, इसमें वेद बंधा हुआ नहीं, अपितु अर्थ के अनुसार भी स्वर वेद में हो सकता है, यह नियम है। ◾️(१०) काव्य के अङ्गभूत श्लेष प्रादि अलङ्कारों का उपययोग इस वैदिक काव्य में सर्वप्रथम आचार्य दयानन्द ने ही किया है, और उन अलङ्कारों के द्वारा अर्थों में बहविध वैचित्र्य दर्शाया है। ◾️(११) वेद में अनित्य (अर्थात् व्यक्ति, जाति, देशविशेषों का) इतिहास नहीं, अपितु उसमें प्रकृति के औपचारिक वा आलङ्कारिक वर्णन है, ऐसा निरूपण किया गया है, जिसमें आज तक की परम्परा साक्षी है। तदनुसार इन्द्र, कण्व, अङ्गिरा आदि किन्हीं व्यक्ति-विशेषों के नाम नहीं हैं। ◾️(१२) इस भाष्य में 'देवता' को मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय माना है तथा इन्द्र, मित्र, वरुण, प्रभृति सब देवतावाची शब्द उसी एक महान आत्मा परब्रह्म जगदीश्वर की विभूतियों के वाचक हैं; (जैसा निरु० ७।४ में माना है)।- ऐसा मानकर यौगिकवाद के आधार पर अनेक अर्थ दर्शाये गए हैं। सर्वानुक्रमणी से भिन्न कहीं-कहीं वाच्यार्थ को देवता मान कर मन्त्रों की व्याख्या की गई है। ◾️(१३) इस भाष्य में मन्त्रों के छन्द भी प्रायः अनुक्रमणी में कहे गये छन्दों से भिन्न दर्शाये हैं। यह छन्दोभेद भी प्राचीन आर्षपद्धति के मोलिक सिद्धान्त के अनुसार है। ◾️(१४) 'व्यत्यय' [काल, वचन, पुरुष, विभक्ति आदि में परिवर्तन के सिद्धान्त को मानकर ही वेद के विषय में 🔥'सर्वज्ञानमयो हि सः' यह बात ठीक-ठीक प्रमाणित हो सकती है, अन्यथा नहीं। यह सिद्धान्त मानकर अनेक स्थानों में व्याख्या की गई है। ◾️(१५) 🔥'वाक्यं हि वक्तुराधीनम्' [वाक्य का अर्थ बोलनेवाले की इच्छा के आधीन है] के अनुसार मन्त्र के पदों को अन्वय में सम्बद्ध करके अर्थ किया गया है। ◾️(१६) 'यज्ञ' आदि शब्दों से विविध- आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक यज्ञों का अर्थ लिया गया है। केवल भौतिक यज्ञों को लेकर आचार्य दयानन्द का भाष्य समझ में ही नहीं आ सकता। दूसरे शब्दों में समस्त शुभ कर्मों का नाम यज्ञ है- 🔥'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म’ [शतपथब्राह्मण १।७।१।५], न कि हवन कुण्ड में आहति डाल देने मात्र का काम, यह बात समझकर ही इस भाष्य को पढ़ना होगा। ◾️(१७) पिङ्गलछन्दःसूत्रानुसार प्रत्येक मन्त्र के षड्ज आदि स्वर भी इस भाष्य में दर्शाये गये हैं। ◾️(१८) वेद सर्वनन्त्र सिद्धान्त अर्थात् सार्वभौमिक नियमों का प्रति पादन करता है, यह बात इस भाष्य से स्पष्ट विदित होती है। ◾️(१९) दयानन्द-भाष्य में नैरुक्त शैली के अनुसार अनेक ऐसे शब्दों के निर्वचन मिलते हैं, जिनके निर्वचन निरुक्त और ब्राह्मणादि ग्रन्थों में भी उपलब्ध नहीं होते। ◾️(२०) सबसे बड़ी और अन्तिम विशेषता दयानन्द के भाष्य की यह है कि उस में नैरुक्त शैली के अनुसार संस्कृतपदार्थ मन्त्रगत पदों के क्रम से रक्खा गया है और उसमें जहां-तहां मन्त्रों के तीनों प्रकार के अर्थों को लक्ष्य में रखकर निर्वचन तथा अर्थ दर्शाया गया है, जो अन्वय में नहीं हो सकता था। अन्वय को संस्कृतपदार्थ का एक अंश समझना चाहिये, और इस संस्कृत अन्वय का ही भाषार्थ हिन्दी अनुवाद किया गया है, जो भाषा करनेवालों से ठीक-ठीक पूरा हो भी नहीं सकता। इस वेद-भाष्य की इस विशेषता को न समझकर बहुत से सज्जन घबराने लगते हैं। इस का प्रकार समझ लेने से फिर कोई कठिनाई नहीं रहती। यहां पर हम यह कह देना आवश्यक समझते हैं कि जितना भी कोई विद्वान् विद्या के भिन्न-भिन्न अङ्गों का ज्ञाता तथा योगादि दिव्य शक्तियों से सम्पन्न होगा, उतना ही उसको वेदार्थ का भान अधिक होगा। [वेदवाणी, वर्ष १, अङ्क ७] [सम्पूर्ण वेदभाष्य आप 👉🏻 https://www.vedrishi.com/book/sampurn-ved-bhasya-वेदभाष्य-सम्पूर्ण 'वेदऋषि' से घर बैंठे प्राप्त कर सकते हैं।] ✍🏻 लेखक - पदवाक्यप्रमाणज्ञ पण्डित ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु (जन्म- १४ अक्तूबर १८९२, मृत्यु- २२ दिसम्बर १९६४) प्रस्तुति - 🌺 ‘अवत्सार’ ॥ओ३म्॥ [21:03, 31/03/2020] Vivek Arya Delhi: Andrew Jackson Davis 1826-191
Subscribe for latest offers & updates
We hate spam too.